सबसे बड़ा साहस है, झूठे ज्ञान को अस्वीकार करने का साहस यदि आपको ज्ञात नहीं है कि ईश्वर है तो मानने को राजी मत होना “ओशो”


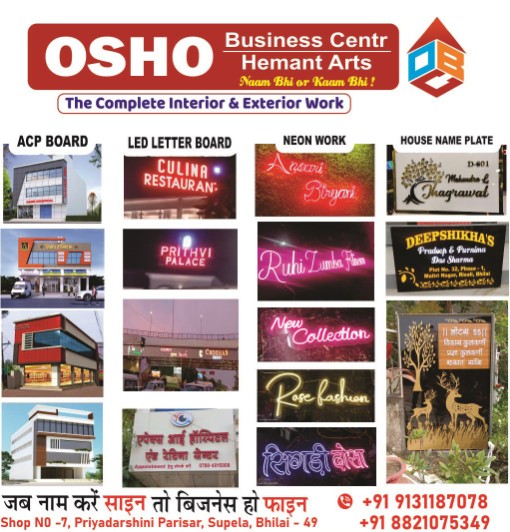 जीवन की क्या परीक्षा है सिवाय जीवन के? और धर्म तो जीवन ही है। इसलिए जो मात्र परीक्षाएं पास करके समझते हैं कि वे शिक्षित हो गए, वे भूल में हैं। वस्तुतः तो जहां परीक्षाएं समाप्त होती हैं, वहीं असली शिक्षा शुरू होती है क्योंकि वहीं जीवन शुरू होता है।
जीवन की क्या परीक्षा है सिवाय जीवन के? और धर्म तो जीवन ही है। इसलिए जो मात्र परीक्षाएं पास करके समझते हैं कि वे शिक्षित हो गए, वे भूल में हैं। वस्तुतः तो जहां परीक्षाएं समाप्त होती हैं, वहीं असली शिक्षा शुरू होती है क्योंकि वहीं जीवन शुरू होता है। धर्म की शिक्षा क्या होगी? हां, धर्म का बीज विकसित हो सके—शिक्षालय इसके लिए अवसर अवश्य ही जुटा सकते हैं। और उस बीज के विकास-पथ की बाधाएं दूर कर सकते हैं। इस अवसर जुटाने में तीन तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं।
धर्म की शिक्षा क्या होगी? हां, धर्म का बीज विकसित हो सके—शिक्षालय इसके लिए अवसर अवश्य ही जुटा सकते हैं। और उस बीज के विकास-पथ की बाधाएं दूर कर सकते हैं। इस अवसर जुटाने में तीन तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमारे तथाकथित धर्म भय का ही शोषण करते रहे हैं और इसीलिए तो आज तक धर्म का भवन खड़ा नहीं हो पाया है। भय की रेत पर भी कहीं भवन बने हैं? और बन भी जावें तो वे कितनी देर टिक सकते हैं?
लेकिन हमारे तथाकथित धर्म भय का ही शोषण करते रहे हैं और इसीलिए तो आज तक धर्म का भवन खड़ा नहीं हो पाया है। भय की रेत पर भी कहीं भवन बने हैं? और बन भी जावें तो वे कितनी देर टिक सकते हैं? नास्तिकता का अर्थ है: अस्वीकार का काल। यदि समाज ईश्वर और धर्म विरोधी है, तो इसके अस्वीकार से गुजरना भी नास्तिकता है। स्वीकृत और माने हुए के अस्वीकार से गुजरना नास्तिकता है। व्यक्तित्व की प्रौढ़ता के लिए यह काल अत्यंत मूल्यवान और लाभप्रद है। जो इससे नहीं गुजरता है, वह सदा के लिए अप्रौढ़ रह जाता है। यह गुजरना साहस और अभय से ही हो सकता है।
नास्तिकता का अर्थ है: अस्वीकार का काल। यदि समाज ईश्वर और धर्म विरोधी है, तो इसके अस्वीकार से गुजरना भी नास्तिकता है। स्वीकृत और माने हुए के अस्वीकार से गुजरना नास्तिकता है। व्यक्तित्व की प्रौढ़ता के लिए यह काल अत्यंत मूल्यवान और लाभप्रद है। जो इससे नहीं गुजरता है, वह सदा के लिए अप्रौढ़ रह जाता है। यह गुजरना साहस और अभय से ही हो सकता है। यही में आपसे भी कहना चाहता हूं। जो व्यक्ति मृत्यु से जितना भयभीत होता है, वह आत्मा की अमरता में उतना ही विश्वास करने लगता है। इस विश्वास का अनुपात और तीव्रता उतनी ही होती है जितना कि उसका भय होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या जीवन के सत्य के प्रति आंखें खोलने को राजी हो सकता है? सत्य का मार्ग अभय के अतिरिक्त और कहीं से भी नहीं जाता है। आत्मा अमर्त्य है, यह भयभीत चित्त का विश्वास नहीं, वरन पूर्ण अभय चेतना का साक्षात्कार है।
यही में आपसे भी कहना चाहता हूं। जो व्यक्ति मृत्यु से जितना भयभीत होता है, वह आत्मा की अमरता में उतना ही विश्वास करने लगता है। इस विश्वास का अनुपात और तीव्रता उतनी ही होती है जितना कि उसका भय होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या जीवन के सत्य के प्रति आंखें खोलने को राजी हो सकता है? सत्य का मार्ग अभय के अतिरिक्त और कहीं से भी नहीं जाता है। आत्मा अमर्त्य है, यह भयभीत चित्त का विश्वास नहीं, वरन पूर्ण अभय चेतना का साक्षात्कार है।