शिक्षालयों से गुजर कर स्वयं की प्रतिभा को बचा लेने से अधिक दुरूह कार्य और कोई भी नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालयों ने मौलिक प्रतिभाओं को नष्ट करने में अपनी कुशलता का चरम बिंदु तो बहुत पहले ही उपलब्ध कर लिया है “ओशो”

ओशो- विचार संग्रह जड़ता लाता है। विचार संग्रह से विचार और विवेक का जन्म नहीं होता है। विचार और विवेक के आविर्भाव के लिए यांत्रिक स्मृति पर अत्यधिक बल घातक है। उसके लिए तो विचार और विवेक के समुचित अवसर होने आवश्यक हैं। उसके लिए तो श्रद्धा की जगह संदेह सिखाना अनिवार्य है।
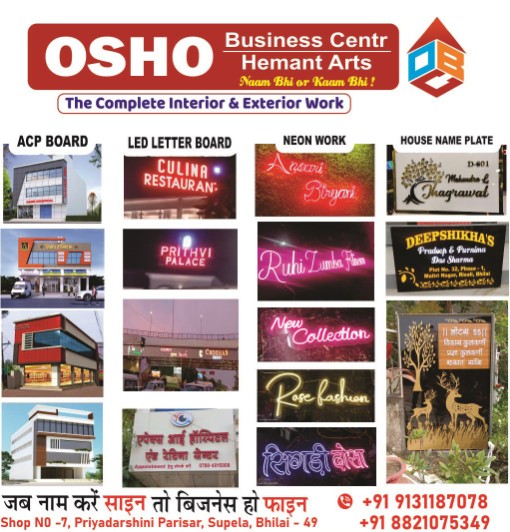 श्रद्धा और विश्वास बांधते हैं। संदेह मुक्त करता है।
श्रद्धा और विश्वास बांधते हैं। संदेह मुक्त करता है।
लेकिन संदेह से मेरा अर्थ अविश्वास नहीं है, क्योंकि अविश्वास तो विश्वास का ही नकारात्मक रूप है—न विश्वास, न अविश्वास वरन संदेह—विश्वास और अविश्वास दोनों ही संदेह की मृत्यु हैं। और जहां संदेह की मुक्तिदायी तीव्रता नहीं है वहां न सत्य की खोज है, न प्राप्ति है।
संदेह की तीव्रता खोज बनती है। संदेह है प्यास, संदेह है अभीप्सा। संदेह की अग्नि में ही प्राणों का मंथन होता है और विचार का जन्म होता है। संदेह की पीड़ा विचार के जन्म की प्रसव-पीड़ा है। और जो उस पीड़ा से पलायन करता है, वह सदा के लिए विचार के जागरण से वंचित रह जाता है।
क्या हममें संदेह है? क्या हममें जीवन के मूलभूत अर्थों और मूल्यों के प्रति संदेह है? यदि नहीं, तो निश्चय ही हमारी शिक्षा गलत हुई है। सम्यक शिक्षा का सम्यक संदेह के अतिरिक्त और कोई आधार ही नहीं है। संदेह नहीं तो खोज कैसे होगी? संदेह नहीं तो असंतोष कैसे होगा? संदेह नहीं तो प्राण सत्य को जानने और पाने को आकुल कैसे होंगे? इसलिए तो हम सब अत्यंत छिछली तृप्ति के डबरे बन गए हैं, और हमारी आत्माएं सतत सागर की खोज में बहने वाली सरिताएं नहीं हैं।
 यह जड़ता किसने पैदा की है? निश्चित ही शिक्षा ने और शिक्षक ने। शिक्षक के माध्यम से मनुष्य के चित्त को परतंत्रताओं की अत्यंत सूक्ष्म जंजीरों में बांधा जाता रहा है। यह सूक्ष्म शोषण बहुत पुराना है। शोषण के अनेक कारण हैं—धर्म हैं, धार्मिक गुरु हैं, राजतंत्र हैं, समाज के न्यस्त स्वार्थ हैं, धनपति हैं, सत्ताधिकारी हैं।
यह जड़ता किसने पैदा की है? निश्चित ही शिक्षा ने और शिक्षक ने। शिक्षक के माध्यम से मनुष्य के चित्त को परतंत्रताओं की अत्यंत सूक्ष्म जंजीरों में बांधा जाता रहा है। यह सूक्ष्म शोषण बहुत पुराना है। शोषण के अनेक कारण हैं—धर्म हैं, धार्मिक गुरु हैं, राजतंत्र हैं, समाज के न्यस्त स्वार्थ हैं, धनपति हैं, सत्ताधिकारी हैं।
सत्ताधिकारी ने कभी भी नहीं चाहा है कि मनुष्य में विचार हो, क्योंकि जहां विचार है, वहां विद्रोह का बीज है। विचार मूलतः विद्रोह है। क्योंकि विचार अंधा नहीं है, विचार के पास अपनी आंखें हैं। उसे हर कहीं नहीं ले जाया जा सकता। उसे हर कुछ करने और मानने को राजी नहीं किया जा सकता है। उसे अंधानुयायी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए सत्ताधिकारी विचार के पक्ष में नहीं हैं, वे विश्वास के पक्ष में हैं। क्योंकि विश्वास अंधा है। और मनुष्य अंधा हो तो ही उसका शोषण हो सकता है। और मनुष्य अंधा हो तो ही उसे स्वयं उसके ही अमंगल में संलग्न किया जा सकता है।
मनुष्य का अंधापन उसे सब भांति के शोषण की भूमि बना देता है। इसलिए विश्वास सिखाया जाता है, आस्था सिखाई जाती है, श्रद्धा सिखाई जाती है। धर्मों ने यही किया है। राजनीतिज्ञों ने यही किया है। विचार से सभी भांति के सत्ताधिकारियों को भय है। विचार जाग्रत होगा तो न तो वर्ण हो सकते हैं, न वर्ग हो सकते हैं। धन का शोषण भी नहीं हो सकता है। और शोषण को पिछले जन्मों के पाप-पुण्यों के आधार पर भी नहीं समझाया और बचाया जा सकता है।
 विचार के साथ आएगी क्रांति—सब तलों पर और सब संबंधों में—राजनीतिज्ञ भी उसमें नहीं बचेंगे और राष्ट्रों की सीमाएं भी नहीं बचेंगी। मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने वाली कोई दीवाल नहीं बच सकती है। इससे विचार से भय है, पूंजीवादी राजनीतिज्ञों को भी, साम्यवादी राजनीतिज्ञों को भी। और इस भय से सुरक्षा के लिए शिक्षा के ढांचे की ईजाद हुई है। यह तथाकथित शिक्षा सैकड़ों वर्षों से चल रहे एक बड़े षडयंत्र का हिस्सा है। धर्म पुरोहित पहले इस पर हावी थे, अब राज्य हावी है।
विचार के साथ आएगी क्रांति—सब तलों पर और सब संबंधों में—राजनीतिज्ञ भी उसमें नहीं बचेंगे और राष्ट्रों की सीमाएं भी नहीं बचेंगी। मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने वाली कोई दीवाल नहीं बच सकती है। इससे विचार से भय है, पूंजीवादी राजनीतिज्ञों को भी, साम्यवादी राजनीतिज्ञों को भी। और इस भय से सुरक्षा के लिए शिक्षा के ढांचे की ईजाद हुई है। यह तथाकथित शिक्षा सैकड़ों वर्षों से चल रहे एक बड़े षडयंत्र का हिस्सा है। धर्म पुरोहित पहले इस पर हावी थे, अब राज्य हावी है।
विचार के अभाव में व्यक्ति निर्मित ही नहीं हो पाता है। क्योंकि व्यक्तित्व की मूल आधारशिला ही उसमें अनुपस्थित होती है। व्यक्तित्व की मूल आधारशिला क्या है? क्या विचार की स्वतंत्र क्षमता ही नहीं? लेकिन स्वतंत्र विचार की तो जन्म के पूर्व ही हत्या कर दी जाती है। गीता सिखाई जाती है, कुरान और बाइबिल सिखाए जाते हैं, कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सिखाए जाते हैं—उनके आधार पर, उनके ढांचे में विचार करना भी सिखाया जाता है! ऐसे विचार से ज्यादा मिथ्या और क्या हो सकता है? ऐसे अंधी पुनरुक्ति सिखाई जाती है और उसे ही विचार करना कहा जाता है!
जहां आधार है, ढांचा है, विश्वास और श्रद्धा है, वहां विचार असंभव है। विचार के लिए तो समस्त ढांचों से मुक्त चित्त चाहिए। शिक्षा मन को ढांचे दे और पटरियां दे तो उचित नहीं है। उसे तो ढांचों में मन न ढल पाए ऐसी सावधानी और सजगता देनी चाहिए। उसे तो ऐसा बोध देना चाहिए कि संस्कारों में चित्त परतंत्र न हो पाए और व्यक्ति की स्वतंत्र चिंतन धारा का आविर्भाव भी हो सके।
ध्यान दिया जाए तो यह अवश्य ही हो सकता है। स्वतंत्र चिंतन के बीज तो प्रत्येक व्यक्ति में है। अनुकूल सुविधाओं में वे विकसित भी हो सकते हैं। स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता है? स्वयं का विवेक और विचार कौन नहीं चाहता है? लेकिन यदि शिक्षा का पूरा यंत्र ही मनुष्य की स्वतंत्रता की जगह परतंत्रता के लिए तैयारी करता हो तो बात ही दूसरी है। तब तो वे थोड़े से व्यक्ति ही आश्चर्य का कारण हैं जो इस यंत्र से गुजर कर भी यंत्र बनने से स्वयं को बचा लेते हैं।
 शिक्षालयों से गुजर कर स्वयं की प्रतिभा को बचा लेने से अधिक दुरूह कार्य और कोई भी नहीं है। विश्वविद्यालयों ने मौलिक प्रतिभाओं को नष्ट करने में अपनी कुशलता का चरम बिंदु तो बहुत पहले ही उपलब्ध कर लिया है।
शिक्षालयों से गुजर कर स्वयं की प्रतिभा को बचा लेने से अधिक दुरूह कार्य और कोई भी नहीं है। विश्वविद्यालयों ने मौलिक प्रतिभाओं को नष्ट करने में अपनी कुशलता का चरम बिंदु तो बहुत पहले ही उपलब्ध कर लिया है।
मनुष्य की परतंत्रता के लिए ही अनुशासन पर अत्यधिक बलदिया जाता है। विवेक के अभाव की पूर्ति अनुशासन से करने की कोशिश की जाती है। विवेक हो तो व्यक्ति में और उसके जीवन में एक स्वतःस्फूर्त अनुशासन अपने आप ही पैदा होता है। उसे लाना नहीं पड़ता है। वह तो अपने आप ही आता है। लेकिन जहां विवेक सिखाया ही न जाता हो, वहां तो ऊपर से थोपे अनुशासन पर ही निर्भर होना पड़ता है। यह अनुशासन मिथ्या तो होगा ही। क्योंकि वह व्यक्ति के अंतस से नहीं जागता है और उसकी जड़ें उसके स्वयं के विवेक में नहीं होती हैं। व्यक्ति का अंतःकरण तो सदा भीतर ही भीतर उसके विरोध में सुलगता रहता है।
ऐसे अनुशासन की प्रतिक्रिया में ही स्वच्छंदता पैदा होती है। स्वच्छंदता सदा ही परतंत्रता की प्रतिक्रिया है। वह उसकी ही अनिवार्य प्रतिध्वनि है। स्वतंत्रता से भरी चेतना कभी भी स्वच्छंद नहीं होती है। मनुष्य को स्वच्छंदता के रोग से बचाना हो तो उसकी आत्मा को परिपूर्ण स्वतंत्रता का वायुमंडल मिलना चाहिए। लेकिन हम तो दो ही विकल्प जानते हैं—परतंत्रता या स्वच्छंदता। स्वतंत्रता के लिए तो हम अब तक तैयार ही नहीं हो सके हैं। अनुशासन—दूसरों से आया हुआ अनुशासन भी परतंत्रता है। ऐसा अनुशासन जगह-जगह टूट रहा है तो बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। यह अनुशासन तो टूटेगा ही। यह तो टूटना ही चाहिए। उसके होने के कारण ही गलत हैं। उसकी मृत्यु तो उसमें ही छिपी हुई है। वह तो अराजकता को बलपूर्वक स्वयं में ही छिपाए हुए है। और बलपूर्वक जो भी दमन किया जाता है, एक न एक दिन उसका विस्फोट अवश्यंभावी है।
ऐसा अनुशासन हो तो व्यक्ति चेतना की सारी सहजता और आनंद छीन लेता है; और टूटे तो भी व्यक्ति को खंडहर कर जाता है। बाहर से आया हुआ अनुशासन सब भांति मनुष्य के अहित में है। शिक्षा बाह्यानुशासन से मुक्त होनी चाहिए। उसे तो व्यक्ति में प्रसुप्त विवेक को जगाना चाहिए।
फिर वह विवेक ही आत्मानुशासन बन जाता है। वैसी चर्या में न दमन होता है, न दबाव होता है। वैसी चर्या तो फूलों जैसी सहज और सरल होती है। और जीवन जब स्व-विवेक के प्रकाश में गति करता है तो अराजकता और स्वच्छंदता की संभावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। जहां दमन ही नहीं है, वहां अराजकता और स्वच्छंदता के विस्फोट भी असंभव हैं।
 मैं पूछता हूं कि क्या हम मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बना सकते हैं? स्वतंत्रता में स्वच्छंदता का भय मालूम होता है। क्योंकि हमने मनुष्य को परतंत्रताओं से दबा रखा है, और उसकी आत्मा सदा से ही उन परतंत्रताओं से छूटने को तड़फड़ाती रही है। और जब भी संभव हुआ है, उसने बंधन तोड़े हैं। लेकिन बंधन तोड़ने के प्रयास में वह जिस कटुता, कठोरता और विरोध से भर जाती है, उसके ही कारण स्वतंत्र तो नहीं होती, स्वच्छंद हो जाती है। स्वतंत्रता सृजनात्मक है, स्वच्छंदता विध्वंसात्मक। लेकिन यदि स्वच्छंदता से बचना हो तो स्वतंत्रता के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है।
मैं पूछता हूं कि क्या हम मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बना सकते हैं? स्वतंत्रता में स्वच्छंदता का भय मालूम होता है। क्योंकि हमने मनुष्य को परतंत्रताओं से दबा रखा है, और उसकी आत्मा सदा से ही उन परतंत्रताओं से छूटने को तड़फड़ाती रही है। और जब भी संभव हुआ है, उसने बंधन तोड़े हैं। लेकिन बंधन तोड़ने के प्रयास में वह जिस कटुता, कठोरता और विरोध से भर जाती है, उसके ही कारण स्वतंत्र तो नहीं होती, स्वच्छंद हो जाती है। स्वतंत्रता सृजनात्मक है, स्वच्छंदता विध्वंसात्मक। लेकिन यदि स्वच्छंदता से बचना हो तो स्वतंत्रता के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है।
शिक्षा निश्चय ही ऐसे आधार रख सकती है जो कि मनुष्य को स्वतंत्र बनाए। अनुशासित व्यक्ति अब नहीं चाहिए। स्वतंत्र और स्वयं के विवेक को उपलब्ध व्यक्ति चाहिए। उनमें ही आशा है और उनमें ही भविष्य है।
अनुशासन की प्रणालियों ने क्या किया है? मनुष्य में जड़ता और बुद्धिहीनता लाई है। अनुशासित व्यक्ति जड़ तो होगा ही। असल में जो जितना जड़ है उतना ही अनुशासित हो जाएगा। देखें, यंत्र कितने अनुशासित हैं? विवेक सदा ही ‘हां’ नहीं कह सकता है। उसे ‘नहीं’ कहना भी आना चाहिए। उसके ‘हां’ में भी तभी मूल्य और अर्थ है अब, जब वह ‘नहीं’ कहना भी जानता हो। लेकिन अनुशासन ‘नहीं’ कहना नहीं सिखाता है। वह तो सदा ‘हां’ ही की अपेक्षा करता है। कहा जाए—गोली चलाओ तो गोली चलाएगा। ऐसी जड़ता की शिक्षा के कारण ही तो दुनिया में युद्ध और हिंसा और भांति-भांति की मूर्खताएं चलती रही हैं और चल रही हैं। क्रमशः…….
ओशो आश्रम उम्दा रोड भिलाई-३




