जो मंदिर ईंट-पत्थरों से बनता है, वह हिंदू का हो सकता है, या ईसाई का या जैन का, या बौद्ध का, लेकिन परमात्मा का नहीं

ओशो- मैं सुनता हूं विद्यापीठों में मंदिरों के बनाए जाने की बातें तो मुझे हंसी आती है। क्या मनुष्य इतिहास से कोई भी सबक नहीं सीखता है?
मंदिर, मस्जिद वाले धर्मों ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्या हमें यह ज्ञात नहीं है?
नहीं, धर्म के बाह्य क्रियाकांडों की जरा भी जरूरत नहीं है। वे व्यर्थ ही होते तो भी चल सकता था। वे तो अनर्थ भी हैं। धर्म बाह्य में नहीं है। इसलिए बाह्य की किसी भी भांति की प्रतिष्ठा अधर्म है।
यह सत्य दो और दो चार जैसा बिलकुल स्पष्ट हो जाना अत्यंत आवश्यक है।
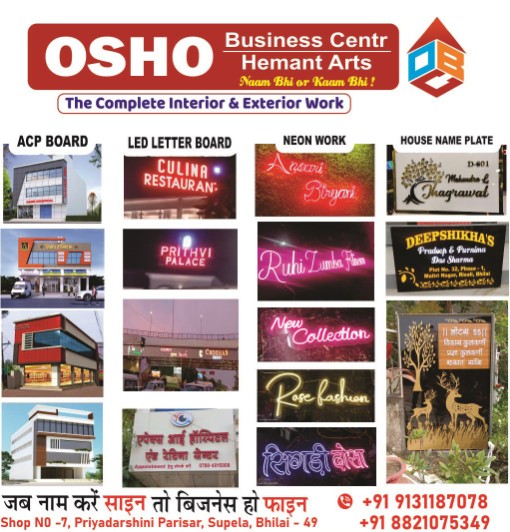 परमात्मा का भी मंदिर है, लेकिन वह ईंट-पत्थरों से नहीं बनता है। और ईंट-पत्थरों से जो बनता है, वह हिंदू का हो सकता है, या ईसाई का या जैन का, या बौद्ध का, लेकिन परमात्मा का नहीं। जो ‘किसी का’ है वह इस कारण ही ‘उसका’ नहीं है। उसके मंदिर की कोई सीमा नहीं हो सकती है क्योंकि वह असीम है। और उसके मंदिर का कोई विशेषण नहीं हो सकता है क्योंकि वह सर्व है।
परमात्मा का भी मंदिर है, लेकिन वह ईंट-पत्थरों से नहीं बनता है। और ईंट-पत्थरों से जो बनता है, वह हिंदू का हो सकता है, या ईसाई का या जैन का, या बौद्ध का, लेकिन परमात्मा का नहीं। जो ‘किसी का’ है वह इस कारण ही ‘उसका’ नहीं है। उसके मंदिर की कोई सीमा नहीं हो सकती है क्योंकि वह असीम है। और उसके मंदिर का कोई विशेषण नहीं हो सकता है क्योंकि वह सर्व है।
निश्चय ही ऐसा मंदिर चेतना का ही हो सकता है। वह मंदिर आकाश में नहीं, आत्मा में है। और उसे बनाना भी नहीं है। वह तो है, सदा से है। बस, उसे उघाड़ना ही है।
इसलिए, शिक्षा से संबंधित धर्म, मंदिर-मस्जिद बनाने वाला धर्म नहीं हो सकता है। वह तो होगा स्वयं में छिपे मंदिर के उदघाटन का धर्म। अंतस में जो है उसे ही जानना है। क्योंकि उसका जानना ही जीवन में एक आमूल क्रांति बन जाती है।
 सत्य को जानना ही जीवन का रूपांतरण है।
सत्य को जानना ही जीवन का रूपांतरण है।
सत्य का, अंतस के सत्य का या परमात्मा का उदघाटन न करने वाली शिक्षा एकदम अधूरी और घातक है। आज तक की शिक्षा की असफलता का कारण भी यही अधूरापन है। जिस युवक को हम अभी विश्वविद्यालयों के बाहर भेजते हैं वह बिलकुल ही अधूरा होता है। उसे जीवन में जो केंद्रीय है, उसका कोई पता ही नहीं होता है। जीवन में जो भी सत्य है, शिव है, सुंदर है, उससे उसकी कोई भी पहचान नहीं होती है। वह केवल क्षुद्र को ही सीख कर आता है और उसमें ही जीता है। निश्चय ही ऐसा जीना आनंद नहीं लाता है और क्रमशः एक अर्थहीनता और रिक्तता और व्यर्थता चित्त को घेरने लगती है। जीवन की धारा इस व्यर्थता के मरुस्थल में खो जाती है और परिणाम में पीछे एक अंधा क्रोध सबके प्रति छूट जाता है। इस क्रोध को ही मैं अधार्मिक मन का परिणाम कहता हूं। धार्मिक मन का फल है, धन्यता और धन्यवाद का भाव। वह समस्त के प्रति कृतज्ञता है। लेकिन वह तो तभी हो सकता है जब जीवन आनंद को पा सके और पूर्णता को। और यह पूर्णता और यह आनंद स्वयं को जाने और पाए बिना असंभव है।
इसलिए, सम्यक शिक्षा धर्मविहीन नहीं हो सकती है। क्योंकि जीवन का आधार जो चेतना है, जो अंतःकरण है, जो आत्मा है, उसे जानना, उससे परिचित होना, जीवन को उसकी पूर्णता तक ले जाने के लिए अपरिहार्य है।
धर्म क्या है?
 मनुष्य के अंतःकरण की शिक्षा ही तो धर्म है।
मनुष्य के अंतःकरण की शिक्षा ही तो धर्म है।
फिर हम क्या सिखाएं? क्या हम धर्मशास्त्र पढ़ाएं? धर्म-सिद्धांत सिखाएं? क्या हम बच्चों को बताएं कि ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है?
नहीं, बिलकुल नहीं। ऐसी कोई भी शिक्षा धर्म की शिक्षा नहीं है। ऐसी शिक्षा भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जाती है। ऐसी शिक्षा भी मनुष्य का पक्षपात ही बन जाती है। ऐसी शिक्षा भी शब्दों-मात्र की सिखावन है। और इससे उस झूठे ज्ञान का जन्म होता है जो कि अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है।
ज्ञान तो केवल वही है जो कि स्वानुभूति से आता है। दूसरों से सीखा ज्ञान, ज्ञान नहीं है। सीखा हुआ ज्ञान, ज्ञान का भ्रम है। और यह भ्रम अज्ञान को छिपा देता है और ज्ञान की खोज बंद हो जाती है। अज्ञान का स्पष्ट बोध शुभ है क्योंकि वह ज्ञान की खोज में ले जाता है। और सीखे हुए ज्ञान को ज्ञान जान लेना बहुत खतरनाक है। क्योंकि उससे मिली तृप्ति पैरों को बांध लेती है और आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है।
मैं एक अनाथालय में गया था। वहां कोई सौ बच्चे थे। व्यवस्थापकों ने मुझसे कहा कि हम यहां धर्म की शिक्षा भी देते हैं। और फिर उन्होंने बच्चों से प्रश्न भी पूछे। पूछा गया, ईश्वर है?—तो उन छोटे-छोटे बच्चों ने हाथ उठा कर हिलाए और कहा: ईश्वर है!—पूछा गया, ईश्वर कहां है?—तो उन्होंने आकाश की ओर इशारे किए! और आत्मा कहां है?—तो उन्होंने अपने हाथ अपने हृदयों पर रखे और कहा: यहां! मैं यह सब नाटक देखता था। व्यवस्थापक बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा: आप भी कुछ पूछिए! मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा: हृदय कहां है? वह यहां-वहां देखने लगा और फिर बोला: यह तो हमें बताया ही नहीं गया है।
धर्म की भी क्या ऐसी कोई शिक्षा हो सकती है? और सीखी हुई बातें दुहराना भी क्या जानना है? काश! बात इतनी आसान ही होती तो क्या दुनिया कभी की धार्मिक न हो गई होती?
 मैंने उस अनाथालय के व्यवस्थापकों और शिक्षकों से कहा था कि आप इन बच्चों को जो सिखा रहे हैं, वह धर्म तो है ही नहीं, उलटे उसके कारण ये जीवन भर के लिए रटे-रटाए तोते बन जाएंगे। और जो व्यक्ति यांत्रिक रूप से किन्हीं बातों को दुहराना सीख जाता है, उसकी बुद्धि को सांघातिक नुकसान पहुंचता है। फिर जीवन जब भी इनके सामने प्रश्न खड़े करेगा—ऐसे प्रश्न जो इन्हें सत्य की खोज में ले जानेवाले हो सकते थे तो वे सीखे हुए उत्तर दुहरा लेंगे और चुप हो जाएंगे। आपकी सिखावन इनकी जिज्ञासा की हत्या है। ये न आत्मा को जानते हैं और न परमात्मा को। और इनके हृदय पर गए हाथ कितने झूठे हैं! और इस झूठ की शिक्षा को आप धर्म की शिक्षा कहते हैं?
मैंने उस अनाथालय के व्यवस्थापकों और शिक्षकों से कहा था कि आप इन बच्चों को जो सिखा रहे हैं, वह धर्म तो है ही नहीं, उलटे उसके कारण ये जीवन भर के लिए रटे-रटाए तोते बन जाएंगे। और जो व्यक्ति यांत्रिक रूप से किन्हीं बातों को दुहराना सीख जाता है, उसकी बुद्धि को सांघातिक नुकसान पहुंचता है। फिर जीवन जब भी इनके सामने प्रश्न खड़े करेगा—ऐसे प्रश्न जो इन्हें सत्य की खोज में ले जानेवाले हो सकते थे तो वे सीखे हुए उत्तर दुहरा लेंगे और चुप हो जाएंगे। आपकी सिखावन इनकी जिज्ञासा की हत्या है। ये न आत्मा को जानते हैं और न परमात्मा को। और इनके हृदय पर गए हाथ कितने झूठे हैं! और इस झूठ की शिक्षा को आप धर्म की शिक्षा कहते हैं?
फिर मैंने उनसे यह भी पूछा था कि आपका स्वयं का जानना भी तो ऐसा ही जानना नहीं है? आप भी तो कहीं सीखी हुई बातें ही नहीं दोहरा रहे हैं? और वे भी वैसे ही यहां-वहां देखते रह गए थे, जैसा कि वह छोटा सा बच्चा हृदय के संबंध में पूछने पर रह गया था। आह! पीढ़ी दर पीढ़ी हम थोथे शब्द सिखाए चले जाते हैं, और उसे ज्ञान समझते हैं। सत्य भी क्या सिखाया जा सकता है? सत्य भी क्या दुहराया जा सकता है।
पदार्थ के जगत में तो सिखाई हुई बातों का कुछ मूल्य है, क्योंकि जो बाहर है उसके संबंध में सूचनाओं से ज्यादा ज्ञान संभव नहीं है। लेकिन, परमात्मा के जगत में उनका कोई भी अर्थ और मूल्य नहीं है, क्योंकि वह जगत सूचनाओं का नहीं, अनुभूतियों का है।
अनुभूति की जा सकती है, उसमें हुआ और जिया जा सकता है, लेकिन उसे सीखा नहीं जा सकता है। उसे सीखना तो मात्र अभिनय बन जाता है। प्रेम क्या कोई सीख सकता है? और यदि कोई सीख कर करे तो वह प्रेम नहीं, बस प्रेम का अभिनय ही तो कर सकेगा। परमात्मा के संबंध में सीखी गई बातें, सिद्धांत, पूजा और प्रार्थना—सब इसलिए अभिनय बन गए हैं। जब प्रेम ही नहीं सीखा जा सकता है तो प्रार्थना कैसे सीखी जा सकती है? प्रार्थना तो प्रेम का ही गहनतम रूप है। और जब प्रेम ही नहीं सीखा जा सकता है तो परमात्मा कैसे सीखा जा सकता है? प्रेम की पूर्णता ही तो परमात्मा है।
 सत्य अज्ञात है और इसलिए जो ज्ञात है—सिद्धांत, शास्त्र, शब्द उन सबसे उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
सत्य अज्ञात है और इसलिए जो ज्ञात है—सिद्धांत, शास्त्र, शब्द उन सबसे उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
अज्ञात में प्रवेश के लिए तो ज्ञात को छोड़ ही देना पड़ता है। ज्ञात से मुक्त होते ही वह सामने आ जाता है जो कि अज्ञात है। इसलिए धर्म सीखने की बजाय अन-सीखना ही ज्यादा है। वह स्मरण की बजाय विस्मरण ही ज्यादा है।
चित्त पर कुछ लिखना नहीं है, वरन सब लिखा हुआ पोंछ देना है। क्योंकि चित्त जहां शब्दों से शून्य होता है, वहीं वह सत्य के लिए दर्पण बन जाता है। चित्त को सिद्धांतों का संग्रह नहीं, सत्य का दर्पण बनाना है। और तब निश्चय ही धर्म-शिक्षा का अर्थ शिक्षा कम और साधना ज्यादा हो जाता है।
धर्म-साधना की तैयारी ही धर्म की शिक्षा है। धर्म की शिक्षा, और विषयों की शिक्षा जैसी नहीं है। इसलिए उसकी परीक्षा भी नहीं हो सकती है। उसकी परीक्षा तो होगी जीवन में, जीवन ही उसकी परीक्षा है। क्रमशः….
ओशो आश्रम उम्दा रोड भिलाई-३




